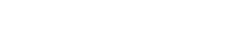रोज़ों का आध्यात्मिक, नैतिक और सामाजिक महत्व
रोज़ों का आध्यात्मिक, नैतिक और...
रोज़ा इस्लाम के पाँच मूल-स्तंभों में से एक है। जो इसकी अनिवार्यता को नकार दे, वह इस्लाम से स्वतः निष्कासित हो जाता है। भोर से संध्या तक ‘अन्न, जल, यौन क्रिया’ छोड़े रहना इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया कि इस्लाम पर “बरक़रार रहना” इस “छोड़े रहने” पर आश्रित हो जाए ? इस प्रश्ना का सादा सा जवाब यह है कि प्रत्यक्षतः खान-पान एवं यौन-क्रिया को तज देने की यह प्रक्रिया इंसान के व्यक्ति त्व से लेकर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को सुधारने और मज़बूत बुनियादों पर निर्मित करने का एक अद्भुयत ईश्वसरीय प्रयोजन है। यह हर ग्यारह महीने बाद क्रियाशील होता है और एक महीने की तपस्या से हर व्यक्तिए को गुज़ारकर अगले ग्यारह महीनों तक उत्तम नैतिक आधारों पर समाज को बनाने और चलाने का प्रावधान कर जाता है। इस्लाम में रोज़े का इतना महत्वपूर्ण स्थान इसलिए है कि यह एक ही समय में व्यक्तिन एवं समाज को, ईश्वरर के आज्ञापालन द्वारा उससे संबंध घनिष्ठर, लाभदायक एवं हितकारी बना देता है।
रोज़े की वास्तविकता
रोज़ा आध्यात्मिक, नैतिक तथा सामाजिक स्तर पर महत्वपूर्ण कैसे है, यह जानने के लिए संक्षेप में रोज़ों की वास्तविकता को समझ लेना सहायक होगा। ‘रोज़ा’ के लिए इस्लाम के मूल ईश-ग्रंथ क़ुरआन में ‘सौम’ शब्द प्रयुक्तः हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ है ‘रुक जाना’ और पारिभाषिक अर्थ है ईश्व र की अवज्ञा (नाफ़रमानी), जैसे बुराई, बदी, झूठ, धोखा, परनिंदा, अपशब्द, अत्याचार, निर्लज्जता, हराम कार्य, व्यभिचार, लांछन आदि दोषों एवं दुष्कर्मों से रुक जाना। क़ुरआन (2:183) में रोज़े को अनिवार्य करते हुए इसका मूल-ध्येय ‘तक़वा’ बताया गया है। ‘तक़वा’ का शाब्दिक अर्थ है ‘बचना’ (संयम और आत्म-नियंत्रण) ; और इसका पारिभाषिक अर्थ है : उपर्युक्त दोषों एवं दुष्कर्मों से बचना। इसके लिए रोज़ों का एक महीना ईश्व रीय प्रावधान से व्यक्तित एवं समाज के लिए संयम एवं आत्म-नियंत्रण का ‘प्रशिक्षण मास’ बनाया गया है।
रोज़े का आध्यात्मिक महत्व
सारे जीवधारियों में ‘शरीर’ और ‘प्राण’, दो मूल तत्व होते हैं, परन्तु मनुष्य में एक तीसरा तत्व ‘आत्मा’ का भी होता है, जो मनुष्य को सारे जीवधारियों से उत्तम, उत्कृष्टद एवं श्रेष्ठए बनाता है। शरीर और आत्मा का धारक इंसान उत्तम तथा लाभकारी उसी वक़्तस बन सकता है जब उसके आध्यात्मिक विकास और दृढ़ता के प्रावधान को उसकी शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी होने के प्रावधान से अधिक महत्व प्राप्तस हो। आध्यात्मिकता का उद्ग म, स्रोत और केन्द्र ‘ईश्वसर’ है। इंसान और समाज जितना अधिक ईशपरायण होगा, ईश-संवेदनशीलता तथा ईश-चेतना उसमें जितनी ज़्यादा तथा सक्रिय होगी, मनुष्य का चरित्र उतना ही श्रेष्ठ- होगा और ऐसे मनुष्यों से बना समाज उतना ही शान्तिमय, न्यायपूर्ण एवं परोपकारी होगा। रोज़े की अद्भु त प्रभावशीलता ऐसे इंसान और समाज बनाने में अति सहायक होती है।
ईश्वपर से घनिष्ठ संबंध इंसान के व्यक्तिनत्व के आध्यात्मिक पहलू का प्रारूपण, संचालन, विकास तथा क्रियान्वयन करता है। रोज़ेदार इंसान हर क्षण मानसिक एवं मनोवैज्ञानिक रूप से जागृत एवं सजग रहता है कि ईश्वपर उसे देख रहा है। प्यास से बदहाल हो तब भी कुल्ली करते समय एक घूँट----बल्कि एक बूँद भी----पानी कण्ठ से नीचे उतरने न देने का आत्मिक बल ईश्व र से आध्यात्मिक संबंध मज़बूत करने में सफल बना देता है। कोई भी देख न रहा हो, किसी को भी मालूम न होने पाए और रोज़ेदार एकांत में खाना-पानी ले सकता है; पति-पत्नी यौन-संबंध से आनंदित हो सकते हैं, लेकिन फिर भी मात्र इस कारण से रुके रहते हैं कि ईश्वरर ने रुके रहने का आदेश दिया है। ऐसे क्षण बार-बार आते हैं और ईश-चेतना एवं ईशपरायणता की पराकाष्ठाश तक रोज़े को पहुँचाते रहते हैं। खाना, पीना और यौन-क्रिया, ईश्वलर की सृष्टिफ-योजना का मूल तथा अभाज्य अंग है, वैध, हलाल तथा अभीष्टा हैं। इन्हें भी रोज़े की हालत में अवैध, हराम, वर्जित करके ईश्वार इंसान में यह प्रेरणा उत्पन्न कर देता है कि ईश्वधर का आदेश होने पर हलाल चीज़ें (भोजन-पानी) और हलाल काम (यौन-क्रिया) भी हमने छोड़ दिया तो जिन ग़लत, बुरे क्रिया-कलापों और चीज़ों से उसने रोक दिया है, उन्हें छोड़ देना तो हमारे लिए बहुत आसान है।
रमज़ान के महीने में अधिक से अधिक इबादत, क़ुरआन पाठ; मन-मस्तिष्क, भावनाओं, इच्छाओं पर नियंत्रण, ईशाज्ञापालन में तत्परता, ईश्वहर की प्रसन्नता अर्जित करने, मृत्यु-पश्चाात स्वर्ग प्राप्तं करने की ललक तथा हर क्षण सत्य-निष्ठा् का लगातार प्रशिक्षण इंसान तथा समाज के आध्यात्मिक स्तर को निरन्तर विकसित करता रहता है, जिसका लाभ व्यक्ति तथा समाज अगले ग्यारह महीनों तक उठाता रहता है।
रोज़े का नैतिक महत्व
नैतिकता इंसान की बहुमूल्य संपत्ति (asset) है। ईश्वेर ने इसी लिए इंसानों की मूल-प्रकृति (instinct) में सारे नैतिक मूल्य सृजित कर दिए और उन्हें इस स्वभाव पर पैदा किया कि ‘करने के कामों’ (Do's) और ‘न करने के कामों’ (Don'ts) की समझ तथा इच्छा-शक्तिन उनकी प्राथमिकता बना दी। जिन कामों में नैतिक गुण हैं (जैसे सच बोलना, परोपकार, न्याय-प्रियता, पर-सेवा भाव, सत्य-निष्ठान, ईमानदारी, अमानतदारी आदि) उनके प्रति तत्परता, और जिन कामों में नैतिक दोष हैं (जैसे झूठ, धोखा, अन्याय, अत्याचार, चोरी, व्यभिचार, अश्लीतलता, क्रूरता, शोषण आदि) उनके प्रति दूरी एवं परिहार (avoidance) बरतना मानव-स्वभाव को अंग बना दिया।
लेकिन कुछ आंतरिक कारणों और कुछ वाह्य कारकों से मूल नैतिक गुणों में ह्रास एवं विघटन होने लगता है। इंसान की इच्छा-शक्तिक इस विघटन को रोक नहीं पाती तथा उसका मनोबल बुराई की तीव्र गति के समक्ष ठहर नहीं पाता। तब फिर ऐसा विकार उत्पन्न होता है जो नैतिक गुणों को ऐसे खा जाता है जैसे ज़ंग, लोहे को। ऐसी स्थिति के लिए विशुद्ध ईश्व रीय धर्म ने अनेक प्रावधान किए हैं, उनमें से एक ‘रोज़ा’ है। यह don’ts से रुकने और do’s को करने का, एक मास का प्रचुर प्रशिक्षण कार्यक्रम है।
इस्लाम के पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सo) का एक प्रसिद्ध आदेश है : ‘किसी व्यक्तिि ने रोज़ा रखकर भी झूठ और बुरा बोलने से स्वयं को न रोका तो अल्लाह को इस से कोई दिलचस्पी नहीं कि वह भूखा-प्यासा रहा।’ (भावार्थ)।। इस संक्षिप्तस सी शिक्षा में ‘झूठ बोलना’ प्रतीकात्मक शैली में कहा गया है। इसका वास्तविक अभिप्राय हर वह ग़लत बात या काम या आचरण है जिसे मूल नैतिक मूल्य के तौर पर इंसान की मूल-प्रकृति ना-पसंद करती है और विशेषतः सत्यधर्म की शिक्षाओं एवं आदेशों में ईश्व र ने जिससे ‘रुक जाने’ (अर्थात् ‘सौम’, रोज़ा), तथा ‘बचने’ (अर्थात् ‘तक़वा’...रोज़े का अस्ल मक़सद) को कहा है। इस तरह ज़रा सी गहराई में उतरकर देखने और विचार करने से बात सरल रूप में समझ में आ जाती है कि ईश्वसर अपने बन्दों से अत्यधिक प्रेम करने के बावजूद उन्हें 29-30 दिनों तक भूख-प्यास से गुज़ारकर वास्तव में उनके नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान का प्रयास करता है।
रोज़े का सामाजिक महत्व
इस्लाम की तीन अन्य इबादतों (मूल स्तंभों)....नमाज़, ज़कात, हज.....की तरह रोज़े की अनिवार्य इबादत का आध्यात्मिक एवं नैतिक महत्व के साथ-साथ सामाजिक महत्व भी बहुत है। रोज़े के ज़रिए से इंसान में जो अनेकानेक आध्यात्मिक एवं नैतिक गुण उत्पन्न होते हैं, वे उत्तम एवं आदर्श समाज के निर्माण तथा सामाजिक दोषों एवं दुर्गुणों के सुधार में अपनी भूमिका परोक्षतः तो निभाते ही हैं, प्रत्यक्ष रूप से भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उदाहरणार्थः-
• ख़ुद रोज़ा रखते हुए समाज के लोखों ग़रीब परिवारों के करोड़ों सदस्यों से जुड़ने और उनके प्रति योगदान, सहयोग एवं सहानुभूति के परमार्थ कामों में मुस्लिम समाज एक माह तक व्यस्त रहता है।
• बीमार रहने के कारण रोज़ा न रखने वालों को एक दिन के प्रतिदान में समाज के ग़रीब लोगों को एक दिन दो समय का (तीस दिन रोज़ा छूटे तो तीसों दिन) खाना खिलाने का आदेश है। इस प्रकार समाज में स्वार्थ के दायरे से बाहर निकलने एवं परमार्थ एवं परहित में अग्रसर होने की परम्परा बनती है।
• कोई व्यक्तिए बुरा-भला कहने, अपशब्द बोलने, लड़ाई-झगड़ा करने पर आ जाए तो आदेश है कि प्रतिक्रया में क्रोधित एवं उद्वेलित न हुआ जाए, बल्कि यह कहकर बात टाल दी जाए और वहाँ से हट जाया जाए कि ‘भाई! मैं रोज़े से हूँ।’
• तीस दिन तक रोज़ा रखने की स्थिति में ज़बान से, आँख से, कान से कुछ ग़लत, अनुचित, बुरी बातें बोलने, देखने, सुनने की छोटी-मोटी ग़लतियाँ हो ही जाती हैं। इसके प्रायश्चि त को भी इस्लामी शरीअत ने समाज के निर्धन एवं वंचित लोगों के हितार्थ काम से जोड़ दिया है। आदेश है कि हर व्यक्तिश रोज़े ख़त्म होने और ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले शरीअत द्वारा निर्धारित मात्रा में धन/सामग्री से ग़रीबों को दान दे ताकि वे भी अच्छी तरह ईद की ख़ुशियाँ मना सकें। यह न किया तो चेतावनी दी गई है कि तीस दिन के रोज़ों की तपस्या ईश्वदर तक न पहुँचेगी, अधर में लटकी रहेगी।
• समाज में यौन-अनाचार, चरित्रहीनता एवं व्यभिचार फैलने की प्रवृत्ति पर रोज़ों के माध्यम से स्वाभाविक रूप से रोक लगाने में सफलता मिलती है। वासना, कामेच्छा, यौन-उत्तेजना को नियंत्रण में रखने का ऐसा प्रभावी, एक-मासीय प्रशिक्षण दिया जाता है कि रोज़ा रखते हुए पति-पत्नी भी यौन-क्रिया से दूर रहते हुए संयम एवं आत्म-नियंत्रण अर्जित कर लेते हैं।
उपरोक्तं दो उप-विषयों के अन्तर्गत आध्यात्मिक एवं नैतिक स्तर पर रोज़े इंसान में जो गुण उत्पन्न करते हैं उनका एक अच्छा, सभ्य, शालीन, शान्तिपूर्ण, हितकारी एवं परोपकारी समाज बनाने तथा समाज से बुराइयाँ दूर करने में काफ़ी योगदान होता है।